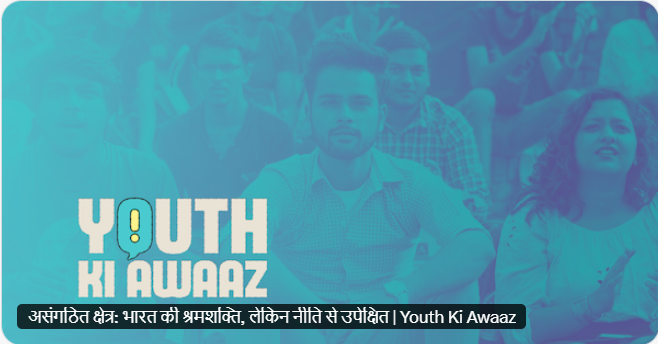
असंगठित क्षेत्र: भारत की श्रमशक्ति, लेकिन नीति से उपेक्षित
डॉ. रमेश कुमार मदान
“भारत की आत्मा उसकी मेहनतकश जनता में बसती है — लेकिन जब यही मेहनतकश असुरक्षित, अदृश्य और असम्मानित हो जाए, तो राष्ट्र की आत्मा घायल हो जाती है।”
भूमिका
भारत की अर्थव्यवस्था को चलाने वाला इंजन अक्सर चमकते कॉर्पोरेट दफ्तरों में नहीं, बल्कि किसानों के खेतों, मज़दूरों की हथेलियों, घरेलू कामगारों के पसीने, और गली-मोहल्लों के हाकरों में छिपा होता है। यही वर्ग है — असंगठित क्षेत्र। यह न केवल देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, बल्कि सामाजिक न्याय, संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक भागीदारी की असली परीक्षा भी।
असंगठित क्षेत्र की व्यापकता
भारत में करीब 90% श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। ये लोग किसी कंपनी या सरकारी सेवा में नहीं, बल्कि छोटे कारोबारों, खेतों, घरों, सड़क किनारे ठेलों, निर्माण स्थलों और अब डिजिटल ऐप्स पर काम करते हैं। इनमें शामिल हैं:
• आंगनवाड़ी, आशा और मिड डे मील कार्यकर्ता
• मनरेगा मजदूर और ग्रामीण श्रमिक
• उबर, ओला, जोमैटो, स्विगी जैसे प्लेटफ़ॉर्म्स पर गिग वर्कर्स
• निर्माण, घरेलू, सफाई और सुरक्षा कार्यकर्ता
• स्ट्रीट वेंडर्स और फुटपाथ व्यापारी
• घरेलू कारीगर, महिला स्व-रोजगारकर्मी और घरेलू उद्योग
• कृषि मजदूर और सीमांत किसान
जमीनी सच्चाई और समस्याएं
इन श्रमिकों की ज़िंदगी रोज़ चुनौती से भरी होती है, लेकिन सरकार, समाज और नीति में उनकी मौजूदगी नगण्य है।
• कोई नौकरी की गारंटी नहीं — आज काम है, कल नहीं।
• सामाजिक सुरक्षा से वंचित — न पीएफ, न बीमा, न पेंशन, न मातृत्व लाभ।
• मजदूरी में दोहरा शोषण — न्यूनतम मजदूरी तक नहीं, समय पर भुगतान नहीं।
• काम की जगह पर असुरक्षा — दुर्घटनाएं आम, लेकिन मुआवज़ा दुर्लभ।
• महिलाओं का त्रैतीयक शोषण — कम वेतन, काम का अनौपचारिक चरित्र और यौन हिंसा का खतरा।
• न्याय तक पहुंच नहीं — न यूनियन, न वकील, न शिकायत प्रणाली।
• डिजिटल भेदभाव — सरकार की स्कीमें हैं, लेकिन जानने और पाने का कोई रास्ता नहीं।
अंतरात्मा को झकझोरने वाले प्रश्न
• क्या भारत की अर्थव्यवस्था केवल उन लोगों की है जो करदाता हैं, या उन लोगों की भी जो अपना खून-पसीना बहाकर व्यवस्था को चलाते हैं?
• क्या नीति केवल संगठित वर्ग के लिए बनेगी, या उन करोड़ों लोगों के लिए भी जो ‘वोट तो देते हैं’, लेकिन ‘आवाज नहीं बना पाते’?
• क्या हम ऐसे विकास मॉडल को स्वीकार करेंगे, जिसमें श्रमिक गुमनाम, अप्रशिक्षित और असहाय हों?
सुधार की राह: केवल योजना नहीं, नीयत भी चाहिए
पहला, राष्ट्रीय श्रमिक पहचान और रजिस्ट्रेशन — ई-श्रम पोर्टल को व्यापकता दें, पंचायत स्तर पर अभियान चलाएं।
दूसरा, सामाजिक सुरक्षा की सार्वभौमिक गारंटी — गिग, घरेलू और कृषि श्रमिकों को बीमा, पेंशन, हेल्थ कवर और आपात सहायता मिले।
तीसरा, महिला श्रमिकों की गरिमा की रक्षा — घरेलू कामगार कानून लागू करें, आंगनवाड़ी वर्कर्स को सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले।
चौथा, डिजिटल सशक्तिकरण और जागरूकता — हर ज़िले में श्रमिक सूचना केंद्र और मोबाइल हेल्पलाइन शुरू हों।
पांचवां, गिग इकॉनमी के लिए नई श्रम नीति — ऐप आधारित कंपनियों को श्रमिक हितों के लिए जवाबदेह बनाएं।
छठा, श्रमिक सहकारिताओं को बढ़ावा — सामूहिक स्वामित्व वाले डिजिटल और स्थानीय मॉडल (जैसे टैक्सी यूनियन, महिला उत्पादक समूह) तैयार किए जाएं।
सातवां, नीति निर्माण में भागीदारी — असंगठित क्षेत्र के प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय और राज्य नीति मंचों में स्थान दिया जाए।
युवाओं के लिए आह्वान
देश के युवाओं से आग्रह है कि वे केवल करियर और कॅम्पस तक सीमित न रहें, बल्कि अपने समाज के उस हिस्से की ओर भी देखें जो आज भी अदृश्य भारत की तरह जी रहा है। अगर हम असंगठित क्षेत्र को संगठित सम्मान न दे सके, तो हमारा लोकतंत्र केवल एक आकृति बन कर रह जाएगा, आत्मा नहीं।
निष्कर्ष
असंगठित क्षेत्र कोई ‘वर्ग’ नहीं, यह भारत का श्रमिक आत्मा है। इस आत्मा को संरचना, सुरक्षा और सम्मान देना हमारा संवैधानिक दायित्व और नैतिक कर्तव्य है। यह कोई दया नहीं — यह अधिकार है। यह कोई योजना नहीं — यह न्याय है।
“जिस भारत ने श्रमिकों के पसीने से देश को खड़ा किया, उस भारत को अब श्रमिकों को सीना तानकर कहने देना होगा — हम सिर्फ मजदूर नहीं, भारत की आत्मा हैं।”
Views: 0


 Previous Post
Previous Post Next Post
Next Post